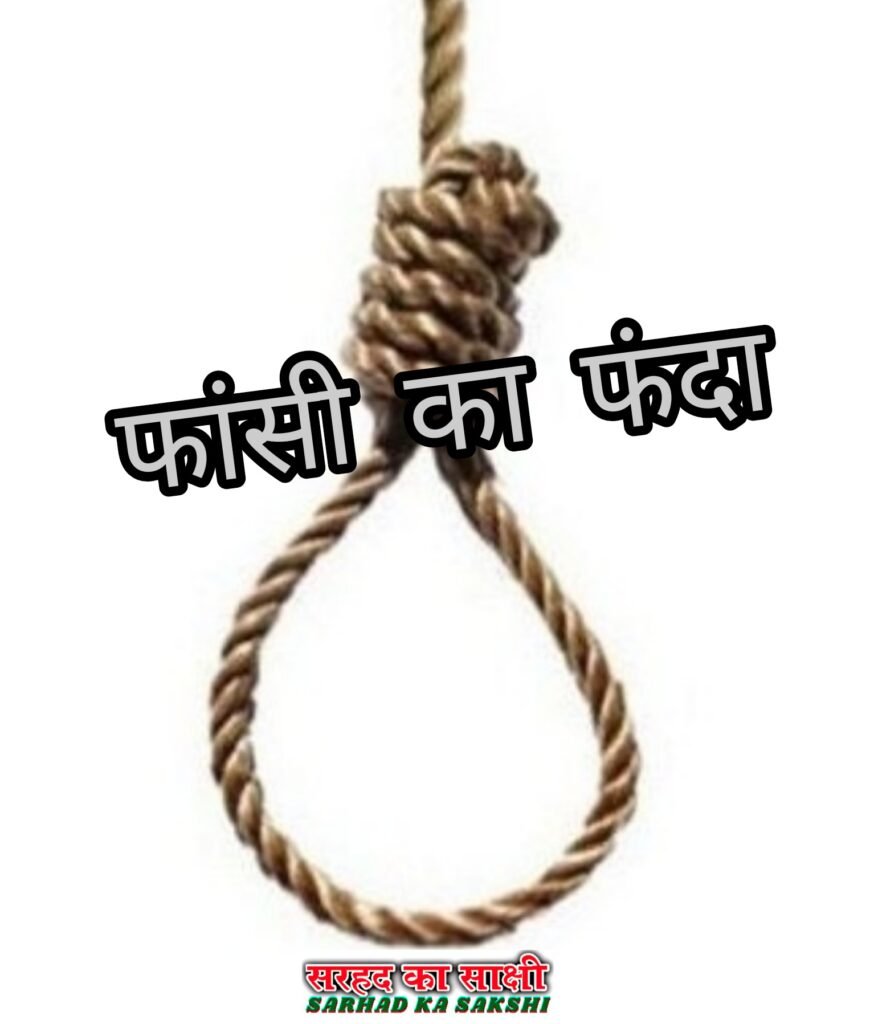यज्ञ -तत्व
सांसारिक आम व्यक्ति के जीवन में यज्ञ की इतनी ही उपादेयता है कि अग्निकुण्ड में कुछ आहुतियां प्रदान करने से मनुष्यों की इच्छित कामनाओं की पूर्ति होती है। असल में कार्य की पूर्ति को देवताओं से जोड़ देना भी सोद्देश्य है। क्योंकि दृश्यमान जगत् में व्यक्ति की आस्था उसे संकुचित बना देती है। कभी- कभी जीवन में ऐसा लगता है कि उसकी कामना की पूर्ति सांसारिक सम्बन्धों के माध्यम् से पूर्ण हो जायेगी, किन्तु जब संसार से असफलता मिलती है तब एक विभिन्न दृष्टि का आगमन होता है। अज्ञात, अदृश्य के प्रति आस्था और श्रद्धा।
जीवन में देवताओं की स्वीकृति का तात्पर्य है- प्रत्यक्ष के साथ-साथ, परोक्ष सत्ता की स्वीकृति। मनुष्य इस विराट ब्रह्मांड का एक अंग है और यह विश्व उतना ही नहीं है, जितना हमें दृष्टिगोचर होता है।
सरहद का साक्षी @आचार्य हर्षमणि बहुगुणा
पौराणिक मान्यता के अनुसार इस विराट विश्व के रचयिता का नाम ब्रह्मा है। संसार में जड़ और चेतन पृथक दिखाई देने पर भी, ये “ब्रह्मा “ के द्वारा एक सूत्र में पिरोये गये हैं। व्यक्ति एक स्वतंत्र इकाई नहीं है, वह तो विराट का एक अंग है।
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, पुरोवाच प्रजापतिः।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष, वोSस्त्विष्टकामधुक ।।
देवान्भावयतानेन ते, देवा भावयन्तु वः।
परस्परं भावयन्तः, श्रेयः परमवाप्स्यथ ।। (गीता ३/ १० ,११ )
प्रजापति ब्रह्मा ने आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर उनसे कहा कि यह यज्ञ तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करनेवाला है। तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं की आराधना करो और वे तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। इसप्रकार एक-दूसरे को उन्नत करते हुए तुमलोग परम कल्याण को प्राप्त करो।
वहिरंग दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है, कि यज्ञ द्वारा प्रकृति के जड़ पदार्थों की पूजा की जा रही है। असल में व्यक्ति इन पंचमहाभूतों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को जड़ मानने का ही अभ्यस्त है। तो क्या चेतन व्यक्ति के द्वारा जड़ पदार्थों की पूजा बुद्धिमानी का काम है? बस यहीं पर यज्ञ का भावनात्मक और तात्विक पक्ष प्रकट होता है। ज्ञान की जिज्ञासाके क्रमिक विकास के अन्तर्गत, जब खोज करते -करते यह पता चलता है कि अगणित ब्रह्माण्डों के मूल में एक ही अव्यक्त सच्चिदानंद तत्व विद्यमान है। अतः चेतन प्रतीत होनेवाला तो चैतन्य ही है, किन्तु जड़ की प्रतीति भी मूल तत्व परब्रह्मपरमात्मा को न देख पाने के कारण ही है। विनय-पत्रिका में इसी तथ्य की ओर इंगित करते हुए कहा गया है, कि यह सम्पूर्ण सृष्टि तो चैतन्य का विलास है। इसे धीर-धीर ही समझा जा सकता है।
रघुपति-भगति-बारि-छालित
चित,बिनु प्रयास ही सूझै।
तुलसीदास कह चिद्-विलास
जग बूझत बूझत बूझै।।
इस मन के विकार कब छूटेंगे, जब श्रीरघुनाथजी की भक्तिरूपी जल से धुलकर चित्त निर्मल हो जायेगा , तब अनायास ही परमात्माका दर्शन होगा। किन्तु तुलसीदासजी कहते हैं, इस चैतन्य के विलासरूप जगत् का सत्य तत्व जो परमात्मा है वह समझते- समझते ही समझ में आयेगा।
एक ईश्वर अनेक रूपों में प्रतिभाषित होता है, यही यज्ञ प्रक्रिया का चरम उद्देश्य है। इस तरह यज्ञ, व्यवहार से लेकर परमार्थ तक पहुंचाने की अद्भुत प्रक्रिया है। यज्ञ कैसे करें, आहुतियां कब प्रदान करें।
यज्ञ करते हुए स्वयं के चित्त को निर्मल करते हुए यज्ञ की प्रक्रिया पर ध्यान देते हुए यज्ञपुरूष को आहुतियां प्रदान करने से यज्ञकर्ता को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है । यज्ञ के संबंध में मुण्डकोपनिषद् के द्वितीय खण्ड के चौथे मंत्र में यज्ञ की अग्नि और अग्नि के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार यज्ञाहुति सम्पन्न होने पर अभीष्ट कामना से किया गया होम पूर्ण फलदाई होता है।
काली कराली च मनोजवा च
सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा ।
स्फुलिंगिनी विश्वरूची च देवी
लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः।। *मुण्डकोपनिषद् ( १ | २ | ४ )
यहां यज्ञाग्नि की सात जिह्वाओं के संबंध में बताया गया है।
यज्ञ की अग्नि की सात जिह्वाओं के नाम इस प्रकार बताये गए हैं-
काली, यह काले रंगवाली है, कराली ये अत्यंत उग्र है, मनोजवा यह मन की तरह अत्यंत चंचल है, सुलोहिता यह सुन्दर लाली लिये लिये हुए है, सुधूम्रवर्णा ये सुन्दर धुएं के से रंगवाली है, स्फुलिंगिनी ये चिंगारियों वाली है तथा विश्वरूचि देवी, यह सब ओर से प्रकाशित, देदीप्यमान।
इसप्रकार यज्ञाग्नि की ये सात तरह की लपटें मानो अग्नि देव की हवि को ग्रहण करने के लिए लपलपाती हुई सात जिह्वायें हैं। अतः जब इसप्रकार अग्निदेवता आहुतीरूप भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार हों, उसी समय भोजनरूप आहुतियां प्रदान करनी चाहिए; अन्यथा अप्रज्वलित अथवा बुझी हुई अग्नि में दी हुई आहुति राख में मिलकर व्यर्थ नष्ट हो जाती है। अतः समस्त साधकों, उपासकों को यज्ञ करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अग्नि में आहुति प्रज्वलित अग्नि में ही डाली जायें। मन्दाग्नि अथवा बुझी हुई अग्नि में आहुतियां न डाली जाएं। विधि पूर्वक किये कर्म का फल कर्ता की मनोकामना को पूर्ण करने में सहायक होता है।
महाराज दशरथ के सकाम यज्ञ में यज्ञ भगवान् यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं हाथ में यज्ञ का प्रसाद चरू लेकर प्रकट होते हैं।
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हें। प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें।।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्दुख भाग भवेत्।।